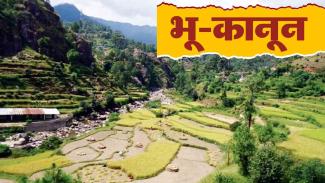उत्तराखंड में जमीन, खेती और भू-कानून
- इन्द्रेश मैखुरी
उत्तराखंड में काफी अरसे से भू-कानून की चर्चा चल रही है. चर्चा में सरकार की तरफ से और सरकार के सामने जो दिखाई दे रहे थे (पता नहीं वो सरकार के सामने है कि नहीं, लेकिन दिखाई दे रहे थे), दोनों तरफ का जुमला एक ही रहा है कि सख्त भू कानून चाहिए!
भू कानून और कथित सख्त वाले भू कानून की चर्चा के इस सिलसिले में समझना जरूरी है कि बात शुरू कहां से हुई.
जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, तब भी यह कहा जाता था कि अलग राज्य का मतलब यह भी है कि जल, जंगल और जमीन पर जनता का अधिकार हो. राज्य जब अपने पच्चीसवें साल में प्रवेश कर चुका है तो यह साफ है कि ऐसा नहीं हो सका!
जमीन के कानून पर बहस का सिलसिला 2018 से नए सिरे से फिर शुरू हुआ जब त्रिवेंद्र रावत भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री थे. वे पहले 6 अक्टूबर 2018 को एक अध्यादेश लेकर आए और फिर 6 दिसंबर 2018 को उन्होंने विधानसभा में कानून पास करके जमीन के कानून में बदलाव किया.
उत्तराखंड में जमीन का जो कानून है, वह उत्तर प्रदेश के समय का ही है. उसका नाम है – ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950’. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में यह सीमा निर्धारित है कि कौन कितनी जमीन रख सकता है. कानून में यह तय है कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती. उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो पहली निर्वाचित सरकार बनी, उसने प्रावधान किया कि कोई बाहर से आकर उत्तराखंड में आवास के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकेगा. 2007 में दूसरी सरकार बनी तो उसने इस सीमा को घटा कर 250 वर्ग मीटर कर दिया. लेकिन यह कानून शहरी निकायों के बाहर ही लागू होता था.
2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस कानून में बदलाव करते हुए प्रावधान कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेगा तो उस पर जमीन की अधिकतम सीलिंग लागू नहीं होगी.
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में धारा 154 में 154 (2) जोड़कर उन्होंने प्रावधान कर दिया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए कितनी भी जमीन खरीदी जा सकती है. उसके अलावा कृषि से इतर उपयोग के लिए भू-उपयोग बदलवाना अनिवार्य कानूनी बाध्यता थी. इस बात का उल्लेख इस कानून की धारा 143 में है. त्रिवेंद्र रावत ने 143 (क) जोड़ कर यह प्रावधान कर दिया कि यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी जाएगी तो उसका भू-उपयोग स्वतः ही बदल जाएगा.
जमीन खरीदने की हदबंदी के खत्म किए जाने का मतलब एक तरह से उस कानून की मूल भावना को ही नष्ट करना था, जिसके नाम में पहली बात ही जमींदारी विनाश है. जमींदारी विनाश या जमींदारी उन्मूलन की यह भावना आजादी के आंदोलन से आई थी. आजादी के आंदोलन से यह मूल्य हमने पाया कि कोई जमींदार नहीं होना चाहिए, कोई असीमित भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए. लेकिन उद्योग लगाने के नाम पर असीमित जमीन खरीदने की अनुमति दे कर नए कॉर्पारेट जमींदार पैदा करने का इंतजाम भाजपा सरकार द्वारा कर दिया गया और एक तरह से आजादी के आंदोलन से हासिल किए हुए मूल्य और कानून की पीठ में खंजर भोंक कर, उसे ध्वस्त कर दिया गया.
2018 से ही जमीनों की बेरोकटोक बिक्री के खिलाफ कानून का सवाल उत्तराखंड में उठता ही रहा है. वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यह जुमला दोहराते रहे हैं कि वे ‘सख्त भू कानून’ लेकर आएंगे. जमीन के कानून के मामले को भी सांप्रदायिक बनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वे गाहे-बगाहे ‘लैंड जेहाद’ का बेसुरा राग अलापते रहे हैं.
बहरहाल बड़े गाजे-बाजे के साथ हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में 21 फरवरी 2024 को वे एक कानून लेकर आए, जो उनके और उनकी पार्टी के अनुसार बहु प्रतीक्षित ‘सख्त भू कानून’ था. हकीकत में यह कोई नया या समग्र कानून था ही नहीं! यह तो उत्तराखंड में लागू उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन अधिनियम मात्र था. उसमें भी कुछ संशोधन ऐसे हैं, जो भूमि के कारोबार को पूर्व में लागू कानून के मुकाबले ज्यादा विस्तारित करते हैं. त्रिवेन्द्र रावत के समय में जो जमीनों की बेरोकटोक खरीद-बिक्री का इंतजाम किया गया था, उसे हरिद्वार और उधमसिंह नगर तक सीमित कर दिया गया है. औद्योगिक प्रयोजन को खरीदने की अनुमति भी जिलाधिकारी नहीं, बल्कि सरकार देगी. लेकिन इसमें सवाल है कि क्या उद्योग लगाने के नाम पर उस हरिद्वार और उधमसिंह नगर की खेती की जमीन की बेरोकटोक लूट होने दी जानी चाहिए, जहां सर्वाधिक उत्पादक खेती होती है? दूसरा पहलू यह है कि इस कानून में किए गए संशोधन नगर निकायों में लागू नहीं होते. उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी जिलों के सभी छोटे-बड़े कस्बों को भी नगर निकाय बना दिया गया है. इसका आशय यह है कि नगर निकाय के रास्ते जमीनों की बेरोकटोक खरीद-बिक्री का रास्ता खुला रखा गया है.
इसके अतिरिक्त धारा 156 में भी संशोधन किया गया है. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में इस धारा में कृषि, बागवानी या पशुपालन का प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लीज पर जमीन देने का प्रावधान है. पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसमें विभिन्न तरह के व्यवसायों को जोड़ते हुए जमीन लीज पर देने का प्रावधान कर दिया है. इसके अलावा कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाने पर उसका भू उपयोग स्वतः बदलने वाला प्रावधान यथावत है.
पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वे ‘सख्त भू कानून’ का जाप करते रहे. अगस्त 2021 में उन्होंने सेवानिवृत्त आईएएस और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए समिति गठित की. 05 सितंबर 2022 को कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. 2023 में पुष्कर सिंह धामी ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में, सुभाष कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक और कमेटी गठित कर दी. और अब 2025 में वे एक संशोधन अधिनियम लाये हैं. जितना वक्त इस प्रक्रिया में लगाया गया, इतने में तो उत्तराखंड की जरूरतों के हिसाब से एक मुकम्मल भूमि कानून बनाया जा सकता था. लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए पुष्कर सिंह धामी तीन-चार धाराओं में संशोधन का अधिनियम ले आए और पूरे राज्य में प्रचार कर दिया कि ‘सख्त भू कानून’ बना दिया गया है.
उत्तराखंड में जमीनों का सवाल किसी भी अन्य राज्य की तरह महत्वपूर्ण है. इसके उत्पादक व लाभकारी उपयोग और बेहतर प्रबंधन की जरूरत है. लेकिन उत्तराखंड में एक हिस्सा जो जमीन के मसले पर आंदोलन कर रहा है, वह इसे बड़े उन्मादी ढंग से देखता है. उनका एक ही राग है कि जमीने नहीं बिकने देंगे. जमीन नहीं बिकें तो इनका क्या उपयोग होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है. इसलिए वे भू कानून के वैसे ही समर्थक हैं, जैसे देश में तथाकथित गौरक्षक गायों के हितैषी बनते हैं!
उत्तराखंड की जमीनों के व्यवस्थित और बेहतर उपयोग के लिए सबसे पहले भूमि बंदोबस्त की जरूरत है. उत्तराखंड में आजादी के बाद 1958 से 1964 के बीच में भूमि बंदोबस्त हुआ था. वह 40 साला बंदोबस्त था जो 2004 में खत्म हो गया. 20 साल उसके बाद और निकल गए लेकिन भूमि बंदोबस्त की सरकारी गलियारों में चर्चा तक नहीं होती. अंग्रेज इस देश में रहे और उत्तराखंड के जितने हिस्से पर उनका कब्जा रहा, वहां 1835 के बाद 132 सालों में उन्होंने 11 बार भूमि बंदोबस्त कराया.
आजाद भारत में जो भूमि बंदोबस्त 1958 से 1964 के बीच में हुआ, उसमें कहा गया था कि पहाड़ में केवल नौ प्रतिशत कृषि भूमि है. यह आंकड़ा 1964 का है. तब से अब तक कितनी कृषि भूमि बची होगी, यह खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है. इसलिए कृषि भूमि के विस्तार और उसके संरक्षण के कानून की आवश्यकता है.
इसके अलावा जो सबसे जरूरी काम किया जाना चाहिए, वह है भूमि सुधार. कृषि भूमि का विस्तार करते हुए भूमिहीन आबादी को भूमि का वितरण एक जरूरी कार्यभार है. पहाड़ में दलित आबादी है, जो मेहनतकश हिस्सा है, लेकिन भूमिहीन है. उसे भूमि का वितरण किया जाना चाहिए.
उत्तराखंड में लोग अक्सर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून चाहिए. लेकिन हिमाचल प्रदेश के कानून का कौन सा हिस्सा चाहिए? हिमाचल प्रदेश के जिस कानून की चर्चा होती है, उसका नाम है – हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971. इस कानून में प्रावधान है कि एक निश्चित अवधि तक हिमाचल प्रदेश में निवास करने के बाद ही वहां जमीन खरीदी जा सकती है. हिमाचल प्रदेश के इस कानून में धारा 118 है जो कहती है कि कृषि भूमि किसी गैर कृषक को नहीं बेची जा सकती.
लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक से पहले हिमाचल प्रदेश ने भी भूमिहीनों को जमीन देने का कानून बनाया. वहां जमीन से जुड़ा एक कानून है, जिसका नाम है – हिमाचल प्रदेश नौतोड़ लैंड रूल्स 1968. यह सरकारी, बेनाप व बंजर जमीन को भूमिहीनों को देने का कानून है.
इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो कानून बना उसका नाम है – हिमाचल प्रदेश होल्डिंग कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1971. यह जमीन की चकबंदी का कानून है.
इस तरह देखें तो हिमाचल प्रदेश में पहले भूमिहीनों को जमीन देने और नयी जमीनें आबाद करने का कानून बना, उसके बाद चकबंदी का कानून बना और फिर भूमि की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला कानून बना. उत्तराखंड में भी भूमि सुधार, संरक्षण और संवर्धन के लिए इसी रास्ते की जरूरत है.
भूमि सुधार के संबंध में कश्मीर का उदाहरण देना भी समीचीन होगा. 1944 में नैशनल कॉन्फ्रेंस ने जो न्यू कश्मीर प्रोग्राम (नया कश्मीर कार्यक्रम) घोषित किया, कृषि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा था. जब जम्मू कश्मीर में नैशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो जो सबसे शुरुआती काम उन्होंने किए, भूमि सुधार उनमें से एक था. भूमि के पुनर्वितरण के जरिये बड़े पैमाने पर भूमिहीनों को जमीनें हासिल हुई. 2011 में योजना पत्रिका में ‘लैंड रिफॉर्म : जम्मू एंड कश्मीर शोज द वे’ शीर्षक से जॉन मैथ्यू का लेख छपा. उक्त लेख में उन्होंने बताया कि जो दादा की पीढ़ी थी वो भूमिहीन थी, लेकिन भूमि सुधार के बाद वर्तमान में जो तीसरे पीढ़ी है, उसमें से 47 प्रतिशत लोग भूमिधर हुए. अतः यह कहा जा सकता है कि कृषि भूमि का विस्तार किए बिना तथा भूमि सुधार किए बिना किसी जमीन के कानून की बात बेमानी है. उत्तराखंड के बंजर होते खेतों और निर्जन होते गांवों को आबाद करने का रास्ता भी यही है कि खेती को उत्पादक और लाभकारी बनाने के ठोस उपाय किए जाएं.
अभी तो उत्तराखंड में सांप्रदायिक नफरत की खेती ही मजबूत हो रही है. यह विडंबना है कि पेशावर विद्रोह के नायक कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे योद्धाओं का प्रदेश, आजकल नफरत की खेती करने वालों के लिए फलदायी बना हुआ है! जिनकी नीतिहीनता और अदूरदर्शिता के चलते उत्तराखंड के खेत बंजर और गांव निर्जन हो रहे हैं, वे नफरत की खेती को मजबूत करने में रात-दिन लगे हुए हैं. वे चाहते हैं कि उत्तराखंड की जमीनों को बड़े भू भक्षियों और कॉरपोरेट लुटेरों के हवाले कर दें और नफरत की खेती के दम पर वे अपनी सत्ता की जमीन को टिकाए रखें. उत्तराखंड को अपनी जमीन और तमाम संसाधनों को भू भक्षियों व कॉरपोरेट लुटेरों से भी बचाना है और नफरत की खेती का भी समूल नाश करना है.